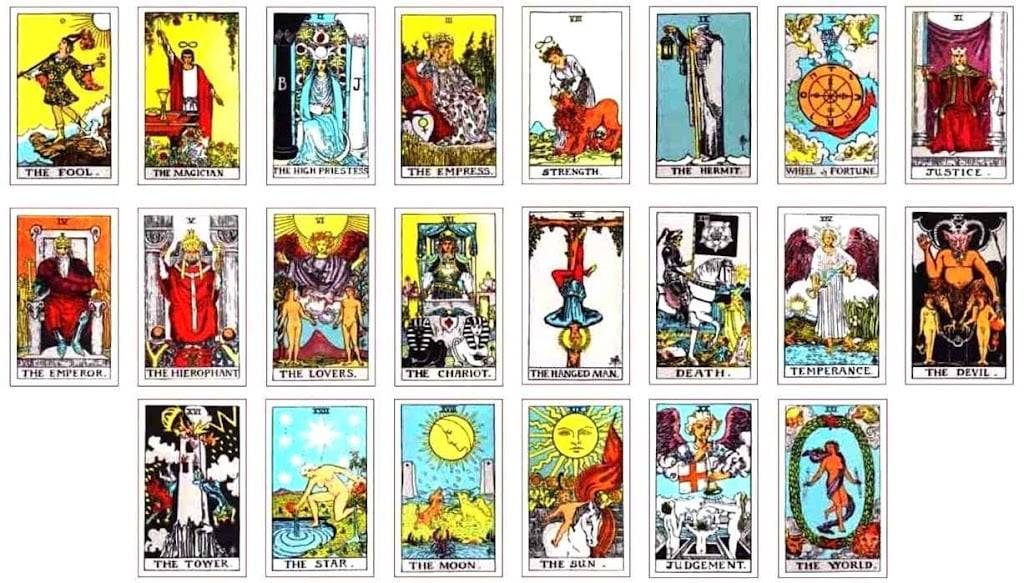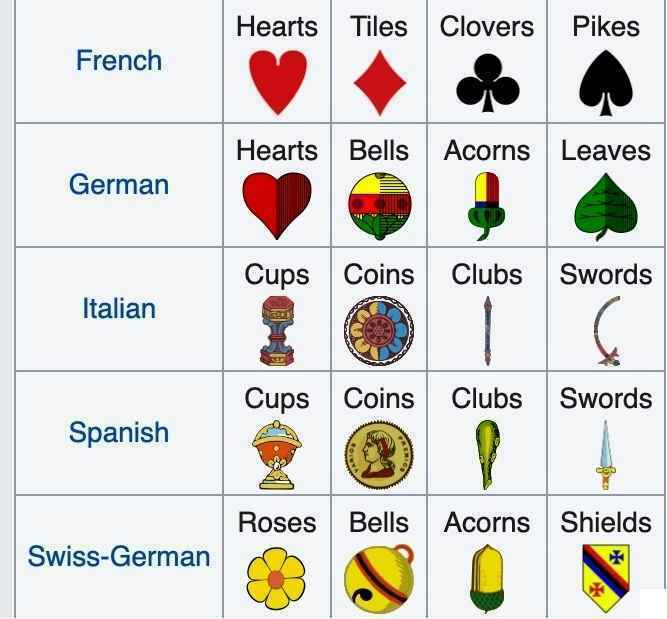रमल ज्योतिष
EPIC Original Story
रहस्य
योग
शरीर के वेग और उसके महत्व | Body Velocity And its Importance
शरीर के वेग और उसके महत्व शरीर के वेगों को कभी नहीं रोकना चाहिए जैस नींद एक वेग है, इसे रोकना नहीं चाहिए क्योंकि वेगों को रोंकने से भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं । हँसी…
तंत्र-मंत्र-यंत्र
ऐसा क्यो ?
उद्योग का इतिहास
घटना का इतिहास
व्यक्ति का इतिहास
पूजा / आरती / व्रत व त्यौहार कथा
आध्यात्म
गंगा में विसर्जित अस्थियां आखिर जाती कहां है | Where do the ashes immersed in the Ganges go
गंगा में विसर्जित अस्थियां आखिर जाती कहां है | Where do the ashes immersed in the Ganges go पतितपावन गंगा को “देव नदी” कहा जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गंगा स्वर्ग से धरती पर…
जीवनी
तेनालीराम की कहानी इन हिंदी
सच्ची घटना पर आधारित मूवी
कुंडलिनी ज्ञान
आठ सिद्धियां कौन-कौन सी है | हनुमान आठ सिद्धियां | अष्ट सिद्धि | aath siddhiyan kya hai
आठ सिद्धियां कौन-कौन सी है | हनुमान आठ सिद्धियां | अष्ट सिद्धि | aath siddhiyan kya hai ‘योग-साहित्य’ में 30 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन है जो साधक को समाधि लगने पर प्राप्त हो जाती हैं । यह अनायास ही होता है । परन्तु साधक को यह भी निर्देश दिया गया है कि इन सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए । अगर अनायास प्राप्त हो ही जाए तो इनका उपयोग सांसारिक सुख-वैभव में नहीं करना चाहिए । यहाँ आठ सिद्धियों का संक्षेप में वर्णन किया जा रहा है । ( 1 ) अणिमा सिद्धि जब योगी इच्छा…